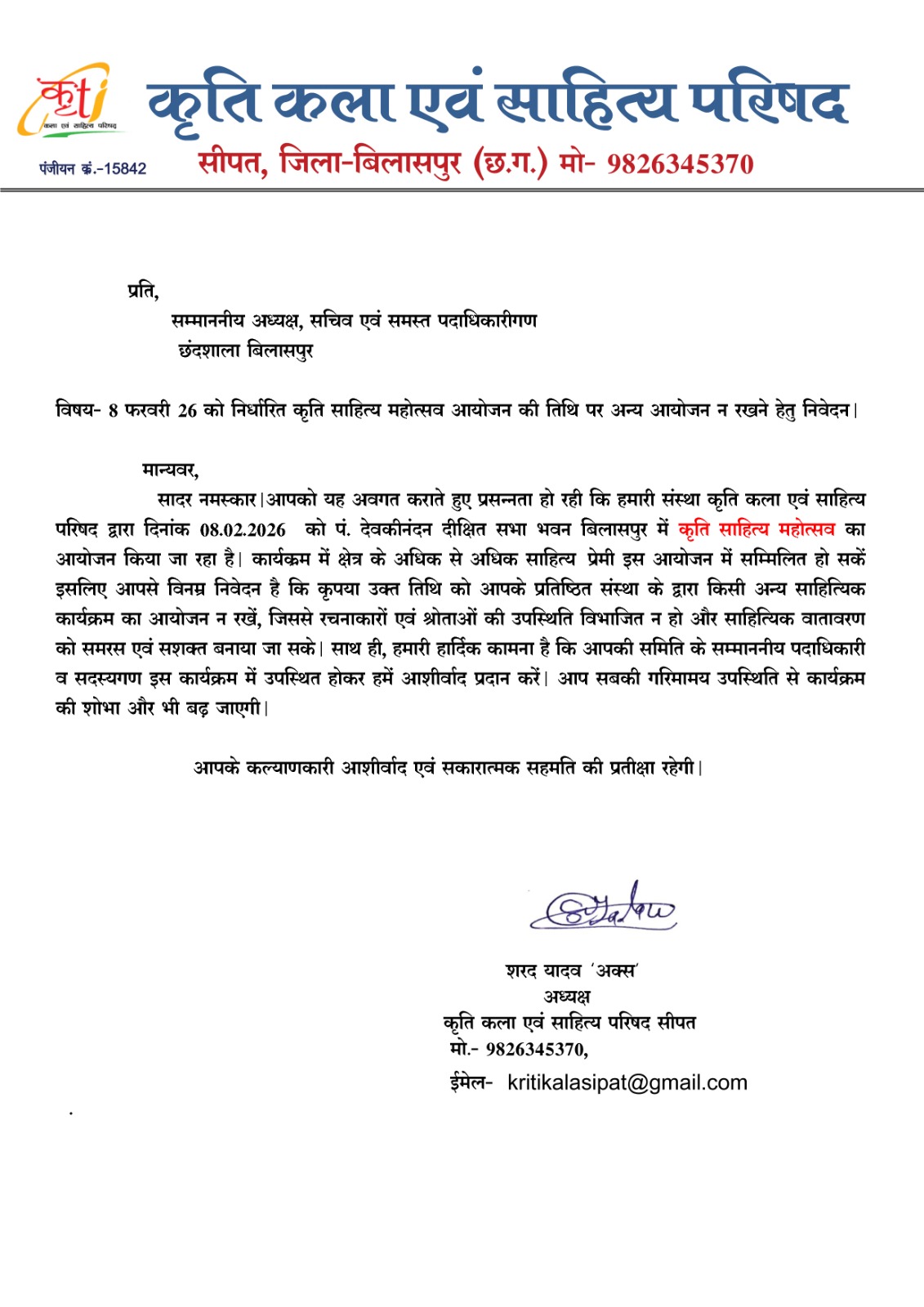बैम्बू पोस्ट | 8 जनवरी 2026 | बिलासपुर
साहित्य अकादमी और केंद्रीय विश्वविद्यालय के साझा आयोजन में साहित्य नहीं, अनुशासन का लाइव डेमो प्रस्तुत किया गया। नाम था—परिसंवाद, स्वरूप था—दरबार, और संदेश था—“विषय पर रहिए, वरना बाहर जाइए।”
कार्यक्रम जैसे ही गंभीरता की कुर्सी पर बैठने ही वाला था, कुलपति महोदय ने दर्शकों की नब्ज़ टटोलते हुए सवाल दाग दिया—
“बोर तो नहीं हो रहे हैं?”
यह कोई मासूम जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि वह संस्थागत हथौड़ा था, जिससे तय किया जाता है कि कौन बोलेगा और कौन बोले ही नहीं।
कथाकार ने साहस दिखाया और कहा—“विषय पर आइए।”
बस, यही वाक्य साहित्य का अनधिकृत वक्तव्य साबित हुआ।
न नारे लगे, न तालियाँ बजीं—सीधे सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हुई और साहित्य को शांति से मंच से उतारकर बाहर पहुँचा दिया गया।
मंच पर बैठे विद्वानों की आँखों में ‘अकादमिक अनुशासन’ ऐसा चमक रहा था, मानो ज्ञान नहीं, नियमावली पढ़ी जा रही हो। उधर सभागार में ‘अभिव्यक्ति की आज़ादी’ अपनी चप्पल ढूँढती रही—जो शायद प्रवेश द्वार पर ही उतरवा ली गई थी।
कुलपति का तर्क पूरी तरह संस्थागत रूप से शुद्ध था—
अगर कार्यक्रम विषय से भटका, तो लेखक भी भटकेंगे।
और लेखक का अपराध भी उतना ही संगीन—
उन्होंने सवाल पूछ लिया, वह भी बिना अनुमति, बिना स्लाइड और बिना पावरपॉइंट।
यह वही समय है जहाँ साहित्य को बोलने से पहले एजेंडा दिखाना पड़ता है, और लेखक को अपनी भाषा से ज़्यादा अपनी कुर्सी की उम्र की चिंता करनी पड़ती है। परिसंवाद अब संवाद नहीं रहा, वह एक अनुशासन शिविर बन चुका है—जहाँ असहमति विचार नहीं, व्यवधान मानी जाती है।
जन संस्कृति मंच ने विरोध दर्ज कराया, साहित्यकारों ने बयान दिए, और विश्वविद्यालय ने वही किया जिसमें वह सबसे अधिक निपुण है—
मौन।
क्योंकि आजकल मौन न केवल सुरक्षित है, बल्कि प्रशासनिक रूप से स्वीकृत भी।
कार्यक्रम अंततः संपन्न हुआ।
चाय समय पर आई, बिस्कुट गिने-चुने बँटे, फोटो खिंचे, रिपोर्ट तैयार हुई—
और साहित्य?
वह एक बार फिर दरवाज़े के बाहर खड़ा रह गया, यह सोचते हुए कि अगली बार मंच पर जाए या सीधे विषय-सूची पढ़कर घर लौट आए।
यह घटना किसी एक लेखक या किसी एक कुलपति की नहीं है।
यह उस व्यवस्था की कहानी है जहाँ साहित्य को मंच तो मिलता है—
बशर्ते वह मंच से सवाल न पूछे,
सोचे नहीं,
और सबसे ज़रूरी—बोर न करे।